दादाजी की कहानी बड़ी ही रोचक थी। छोटी उम्र में ही वो बटवारे के मारे कही से इस इलाके में आ पहुंचे। माँ-बाप का साया उस समय के मज़हबी दंगों में ही उठ गया था। किसी एक मौसी और मौसा के साथ वो एक कैम्प आ पहुंचे। बचपन के एक-दो साल उन्होंने वही कैम्प में गुजारे। कैम्प, जो की निर्वासितों के लिए बनाया गया था, एक अजीब नाम से जाना जाता था - शरणार्थी कैम्प। वहीं से दादाजी की पहचान में ये लफ्ज़ जुड़ सा गया था।
गाव को दो हिस्सों में बाटती हुई वह सड़क एक चौराहे को जा मिलती थी। सड़क के एक तरफ जहाँ बड़े-बड़े मकानों के पिछवाड़े थे, जिनमे बाथरूम और किचन से आने वाला पानी एक नाली में गिरता था। वही सड़क की दूसरी और कुम्हारो की एक बस्ती हुआ करती थी। दिनभर वहा मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हुआ करता था। उस सड़क से गुजरनेवालों को एक तरफ से नाली की, तो दूसरी तरफ मिट्टी के घड़े बनाते समय आनेवाली धुँए की बदबू को झेलना पड़ता था। उसी सड़क पर, चौराहे के बिलकुल पहले, कुम्हारो की बस्ती के नजदीक वह दुकान थी।
दूकान के बाहर छोटे-छोटे डिब्बों में तेल भरा हुआ रहता था। वैसे तो दूकान सभी चीजों की थी, जैसे आम तौर पर राशन की होती है। तेल के डिब्बों से गुजर कर अंदर जाओ तो अँधेरे में दूकान का सारा नक्शा नजऱ आता था। एक काउण्टर जो लगभग साढ़े चार फूट ऊँचा था, एक आम बच्चे को अंदर देखने में बड़ी दिक्कत हो इतना ऊँचा। काउण्टर पर कांच के डिब्बे हुआ करते थे, जिनमे गोली और पेपरमिंट भरें पड़े रहते थे। दूकान के अंदर अलमारियों में अनाज़ की बोरियाँ हुआ करती थी और पिछवाड़े में एक छोटे गोदाम। दुकान और गोदाम को जोड़नेवाली एक छोटी अंधेरी गली थी।
वैसे तो वह दूकान किराने की हुआ करती थी लेकिन कुम्हारो की बस्ती उस दुकान में ज्यादातर खाना बनाने का कच्चा तेल खरीदने जाती थी। शायद दुकानदार की आमदनी भी तेल ही की वजहसे होती होगी। और होती भी कैसे नहीं? उस पुरे इलाक़े में बस वह एक ही दूकान थी जहां राशन तो मिलता ही था मगर तेल थोक में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी।
उस दूकान को खुलते या बंद होते बहोत कम लोगों ने देखा होग़ा। सबेरा होते ही, सड़क पर चहल-पहल के पहले, दूकान खुली नज़र आती थी और देर रात तक वहा कोई न कोई बैठा दिखाई देता था। दूकान खोलना घर के दो बच्चो की जिम्मेदारी हुआ करती थी। दो बच्चे, शायद बारह और चौदा बरस के थे। बड़ी सबेरे स्कूल का बस्ता लिए, घर के कपडे पहने वो दूकान खोलते आते थे। पहले दरवाजों को लगे ताले खोलना, सामनेवाली जगह पर झाडू लगाना, फिर टीन के तेल के डिब्बे एक-एक करके बाहर रखना, दूकान की अंदर सफाई करना और फिर दो बेंच उस टीन के डिब्बों के सामने ला कर रखना ये उन्हीं का काम होता था। करीब आठ बजे उन बच्चों के बापू दूकान संभालने आते थे। साढ़े नौ के करीब उन की माँ हाथ में कई सारे थैले लिए वहां पहुँचती थी। थैलो में बच्चों का खाना, स्कूल के लिए टिफ़िन और परिवार के लिये दोपहर का खाना हुआ करता था। बच्चों की माँ दूकान पर पहुँचते ही अंदर गोदाम और दूकान के बीच वाली जगह में जमीन पर बैठी रहती थी। ज़्यादा तर वही उसकी जगह हुआ करती थीं। उसका काम जरूरत पड़े तो गोदाम से दुकान में सामान लाना था।
ठीक दस बजे घर के सब से बड़े, बच्चों के दादा, दूकान पर पहुंचते थे। उम्र के साथ दादाजी को चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए वह घरसे निकलते तो बहू के साथ ही थे पर पहुँचते ज़रा देरी से। दादाजी पहुँचते पहुँचते दूकान पर गिराहिकों का आना शुरू होता था। वैसे बेटे, बहु, और बच्चों के होते दादाजी शायद ही कभी काउण्टर पर बैठते थे। लेकिन उन के दूकान पर पहुंचते ही परिवार के सब सदस्य चौकन्ने होते थे। बहु घूंघट ओढ़े जमीन पर बैठी और बच्चो के बापू काउण्टर पर नजर आने लगते।
दादाजी के लिए दूकान के आगे, उन टीन के तेलों के डिब्बों के पीछे एक कुर्सी लगायी जाती थी। वही पर वो दिन का ज्यादा समय गुजारते थे। जाड़े के दिन हो तो वहा एक चारपाई हुआ करती थी जिसपर दादाजी दिनभर बैठे या लेटें नज़र आते थे। सामनेवाली सड़क से आते जाते लोगों को टोकना उनकी एक आदत सी हो गई थीं। ज्यादातर लोग उन्हें हस कर टाल देते थे लेकिन दिन में दो चार हम-उम्र उन्हें मिल ही जाते जो उन की सुनने बैठते थे।
दादाजी का बात करने का तरीका बड़ा अज़ीब सा हो चला था। कोई उन्हें पूंछ लेता की वो कहा से इस गांव में आये थे। या फिर अगर किसीने हालात के बारे में पुंछ लिया तो फिर वह कह उठते,
“मेरा गांव बड़ा ख़ूबसूरत था। बड़े बड़े पहाड़ो के बीच, नदी के किनारे। खूब ताज़ी हवा हुआ करती थी।”
जब कोई उन्हें ये याद दिलाता की अब तो ये ही उनका गांव है, तो कह उठते,
“ये कौनसी ताकत है जो कहती है की मैं अपना गांव छोड़ दू? कौन तय करता है की मै अपना गांव छोड़कर यहाँ दूर आ कर बस जाऊँ?”
वैसे दादाजी की कहानी बड़ी ही रोचक थी। छोटी उम्र में ही वो बटवारे के मारे कही से इस इलाके में आ पहुंचे। माँ-बाप का साया उस समय के मज़हबी दंगों में ही उठ गया था। किसी एक मौसी और मौसा के साथ वो एक कैम्प आ पहुंचे। बचपन के एक-दो साल उन्होंने वही कैम्प में गुजारे। कैम्प, जो की निर्वासितों के लिए बनाया गया था, एक अजीब नाम से जाना जाता था - शरणार्थी कैम्प। वहीं से दादाजी की पहचान में ये लफ्ज़ जुड़ सा गया था। पहले इसी वज़ूद की भरोसे उन्हें दो वक़्त की रोटी मिलती थी। पर ये उन्हें बिलकुल ही नहीं पता था की उनकी पहचान सिर्फ़ उन्ही की नहीं बल्कि उनके आनेवाली नस्लों की भी होगी।
जब सरकार ने उन्हें कैम्प से बाहर निकालकर इस छोटे गांव में बसने भेजा, तो वैसे तो उन्हें बड़ी ख़ुशी हुईं। लेकिन एक तरफ बचपन की वो यादे, अपने गांव से बिछड़ने का ग़म उन्हें हमेशा बेचैन करता रहता। अपनी ख़ुद्दारी और मेहनत से, छोटे-छोटे काम कर के उन्होंने एक दिन ख़ुद की एक दूकान शुरू की थी। जगह, वही कुम्हारो की बस्ती के पास, बड़े-बड़े मकानों के पिछवाड़े में। वैसे गांव मे हर दूकान को अपना एक नाम था। जैसे की ‘गुप्ता जनरल स्टोअर्स’। किसीने अपने खानदान का नाम दूकान को दिया था, तो कई दूकानों के नाम कुछ अंग्रेजी लफ़्ज़ों के इस्तेमाल से सजाएं गए थे। दादाजी ने भी दूकान का नाम रख़ा तो था लेकिन उनकी दूकान को सब एकही नाम से जानते थे – ‘शरणार्थी की दूकान’।
उन्हें इस बात का ख़ल था की उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। अपनी ही मुल्क में वह से यहाँ आकर बसने वालों को कैसे कोई शरणार्थी कह सकता है? वह हमेशा सोचते रहते। उम्र बढ़ती गयी, परिवार बढ़ने लगा, कारोबार भी बढ़ने लगा और साथ-साथ वह दुःख भी बढ़ता गया की उन की तीन पीढ़ियों को आज भी उसी नाम से जाना जाता रहा। बल्कि उन के बच्चे और पोते तो इसी गांव की पैदाइश थे। आज के बच्चों को तो उस शब्द का मतलब भी नहीं समज़ता होगा।
दूकान के बाहर कुर्सी पर बैठे या चारपाई पर लेटे वह आस-पास के लोगों से जब बाते करते थे, बात करते कम सुनाते ज्यादा थे, तब उन के अंदर से वह मलाल हमेशा उभर आता था। उम्र के साथ साथ उन की बाते भी एक ही बात दोहराती थी। जैसे ही किसी ने हालात के बारे में पूँछ लिया तो वो कहते थे -
"ये कौनसी ताकतें हैं जो आदमी को आदमी से शरणार्थी बनाती है? मुझे तो अपना गांव पसंद था। वो पहाड़, वो नदी और वो खुली हवा।"
"ये कौनसी ताकत है जो कहती है की मैं अपना गांव छोड़ दू?"
जैसे ही उन्हें कोई समझाने की कोशिश करता तो दादाजी उसी की रट लगाते रहते।
“मै भुला नहीं हूँ। बहोत गुस्सा है मुझ में। उन ताकतों के खिलाफ जो आदमी को रेफ्यूजी बनने पर मजबूर कर देती है।”
अब तो कई साल बीत गए। अब दादाजी भी नहीं रहे। आज भी गांव में अधेड़ उम्र के लोग उन को याद करतें है। कुछ लोग जो तब उन का मज़ाक उड़ाते थे, अब उन की बातों का मतलब समज़ने लगे है।
फिर भी उस दूकान को अब भी उसी नाम से जाना जाता है – शरणार्थी की दूकान।
- सलील जोशी, बोस्टन
salilsudhirjoshi@gmail.com
हेही वाचा :
Tags: hindi story sadhana digital salil joshi refugee camp Load More Tags








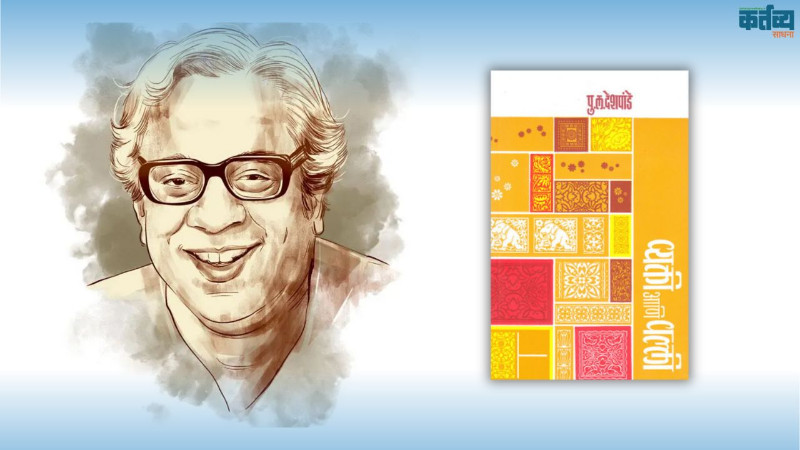



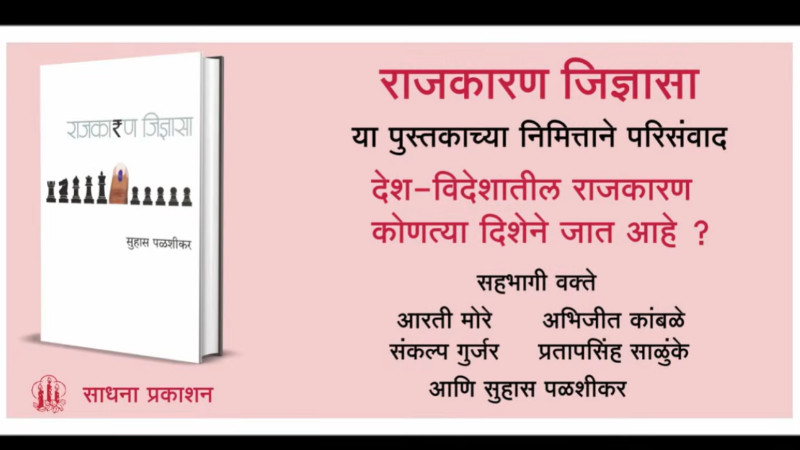

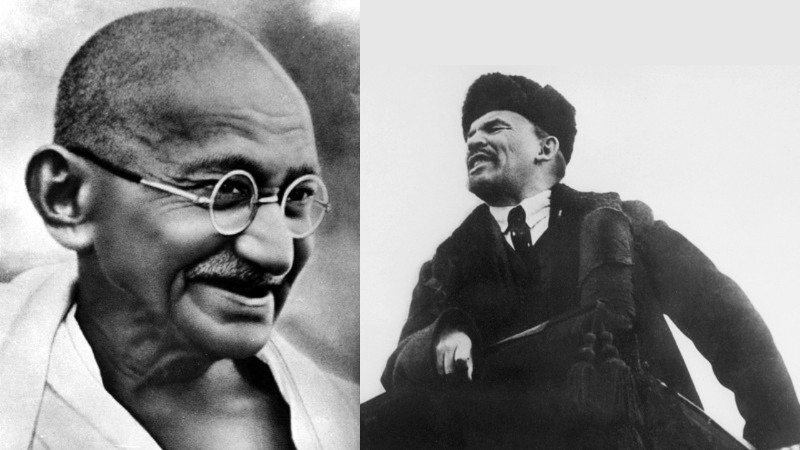



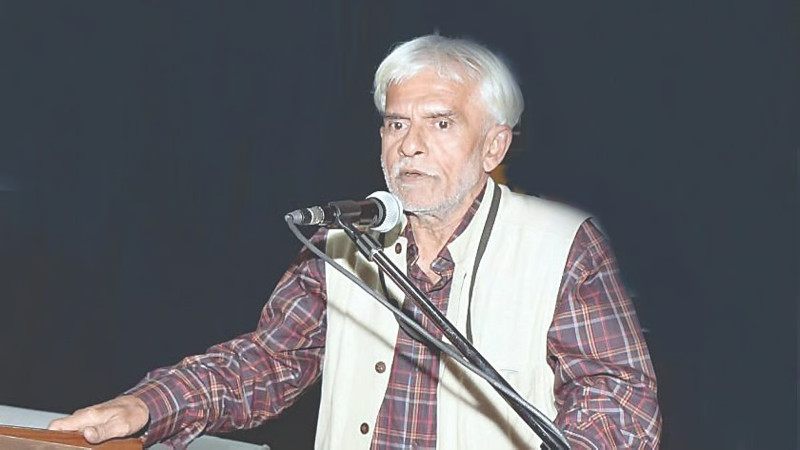

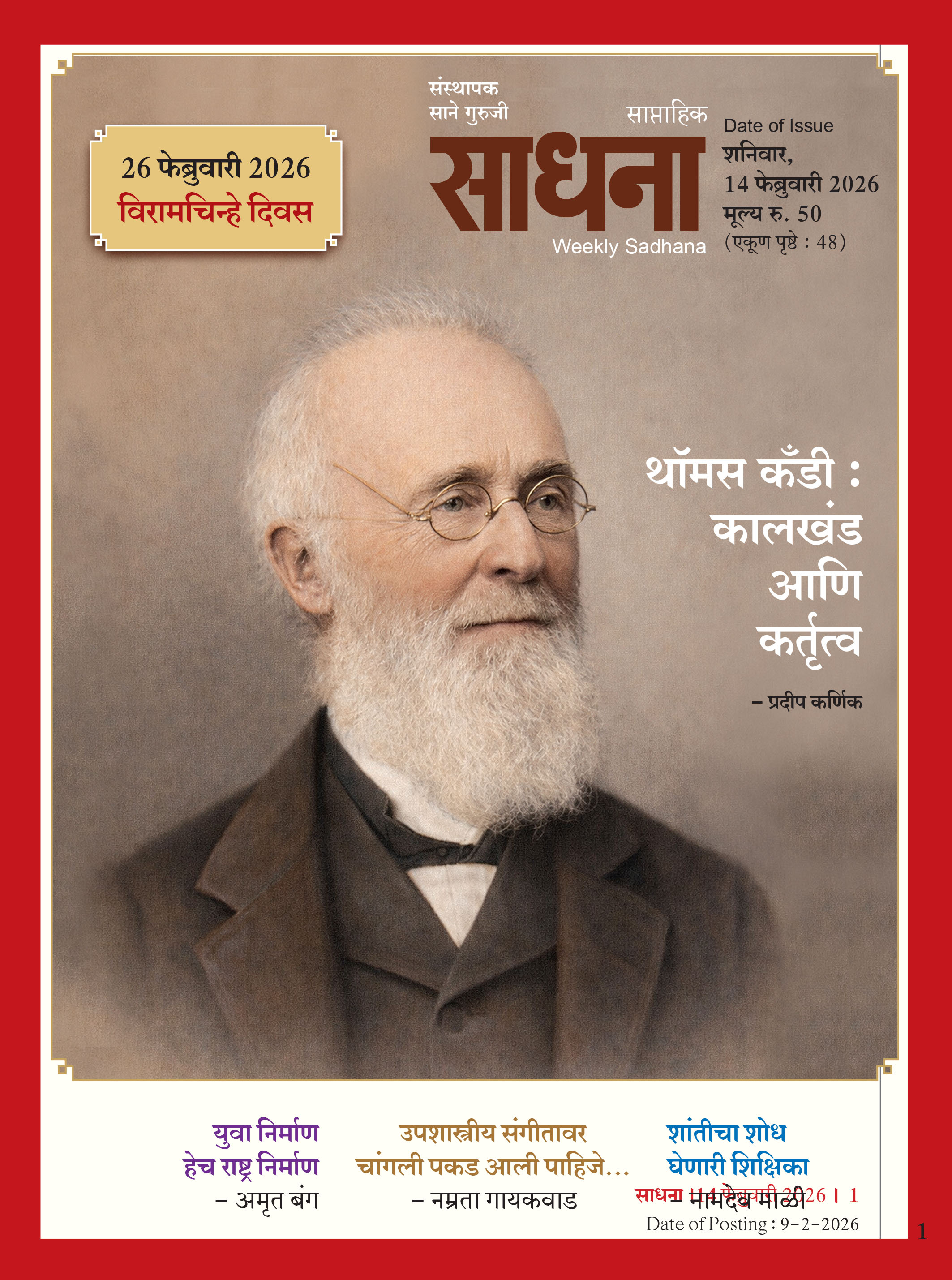



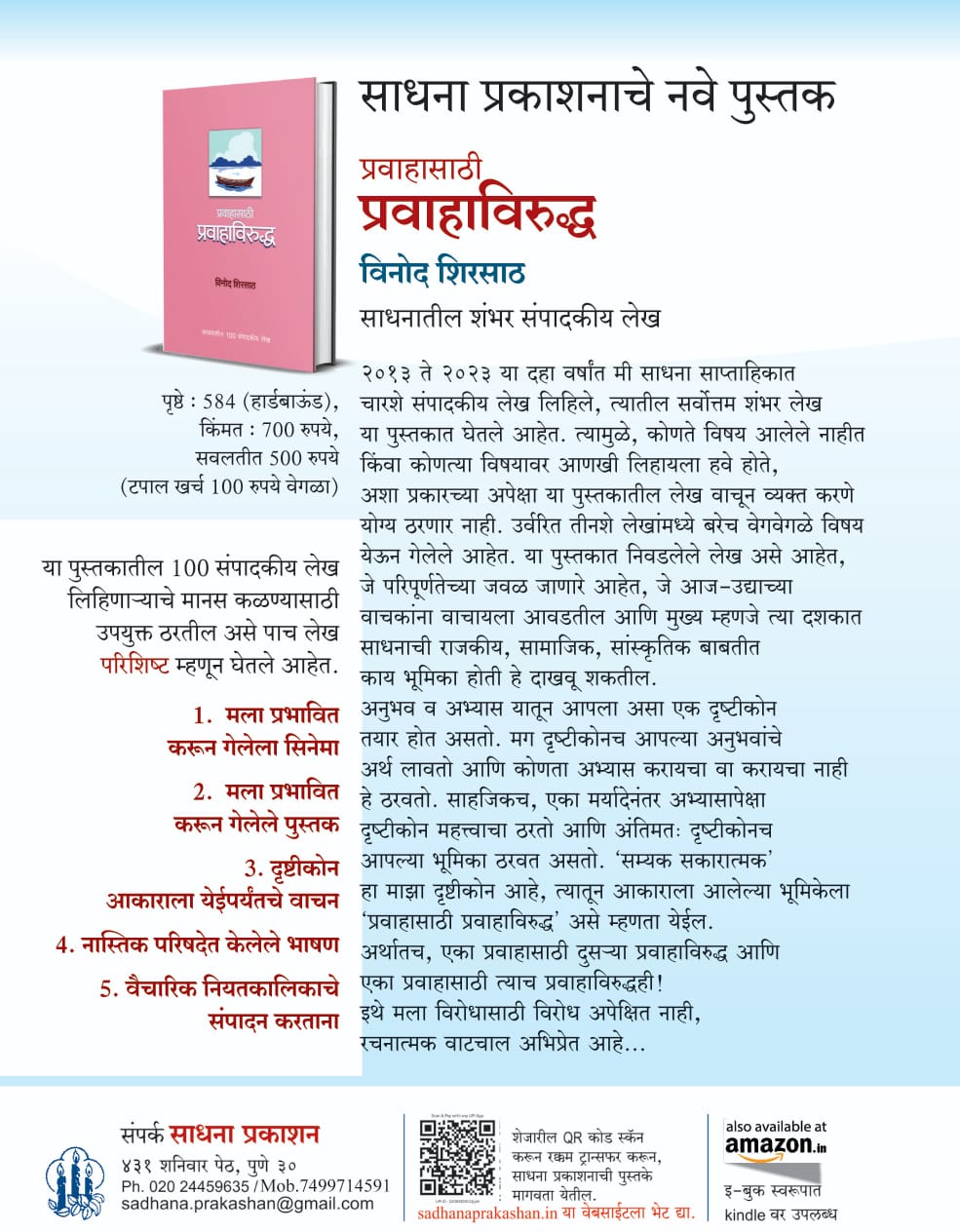

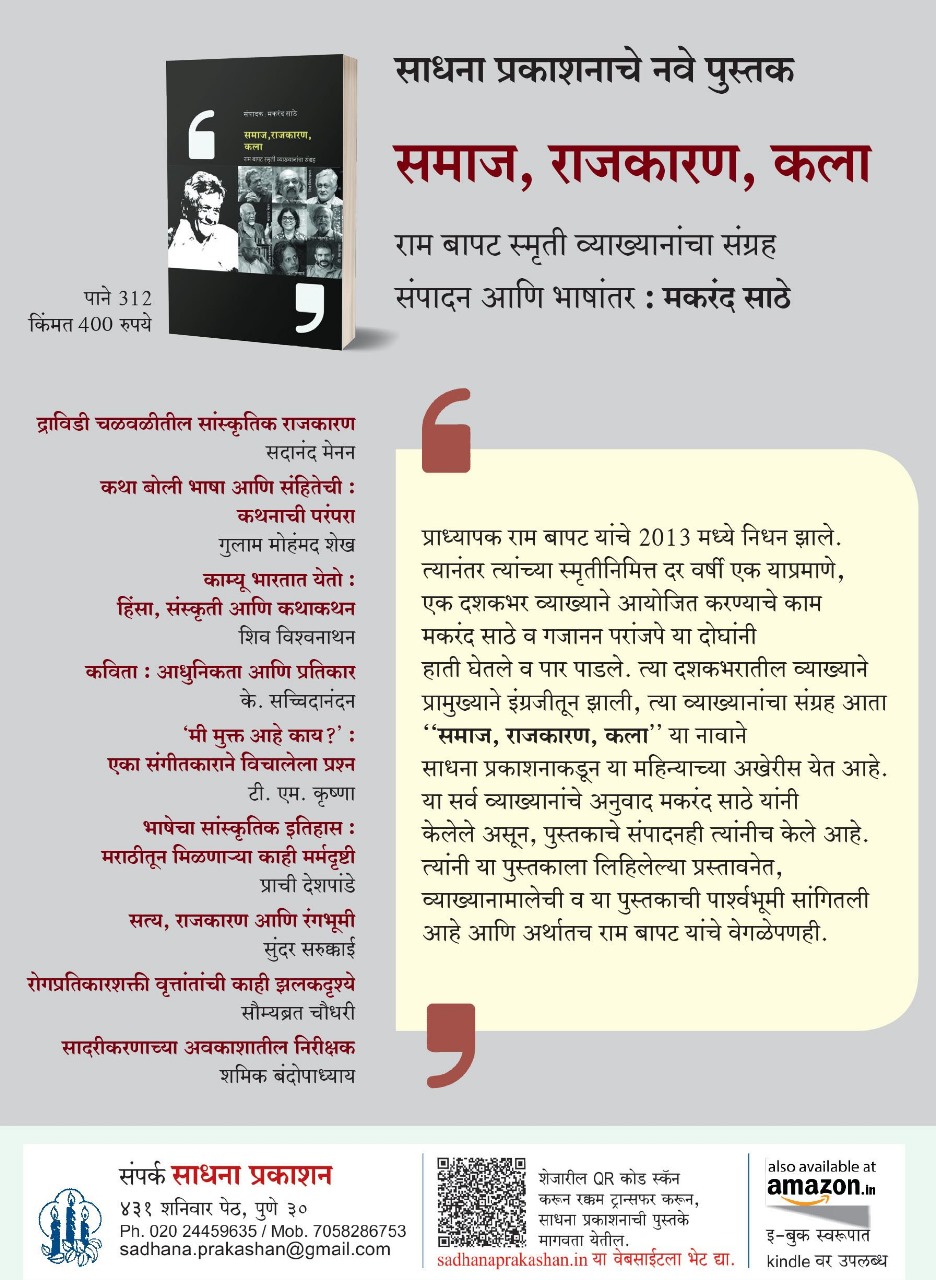

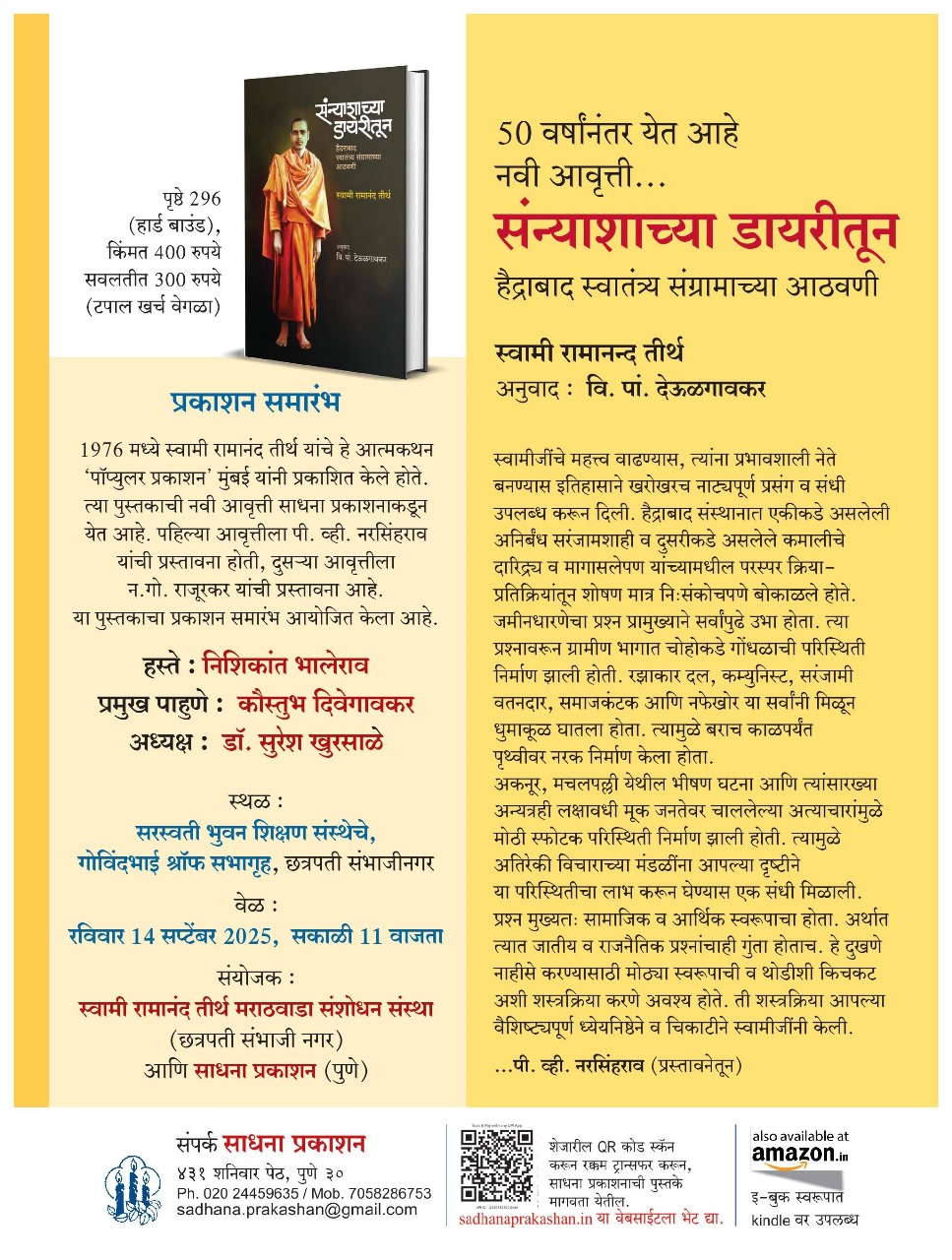
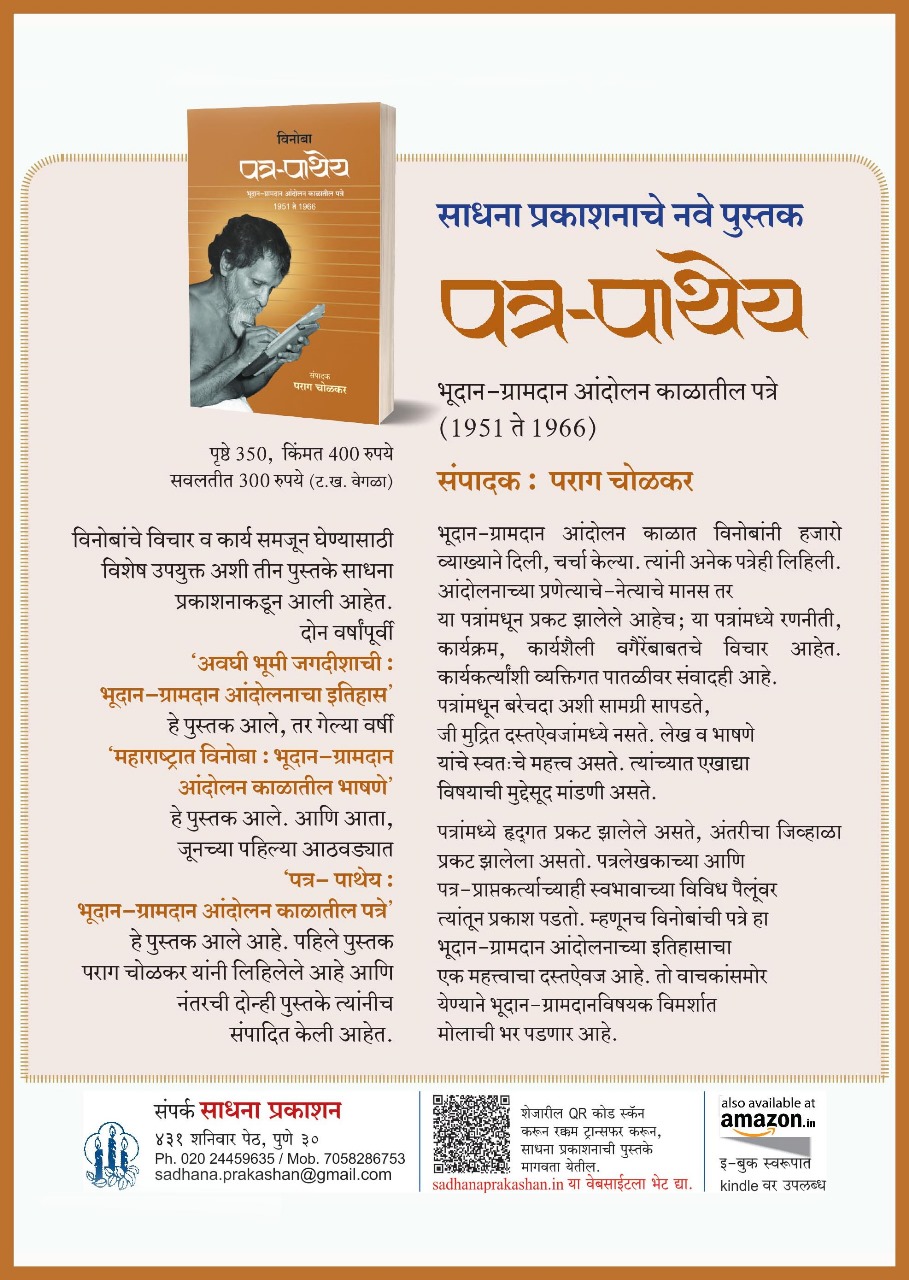


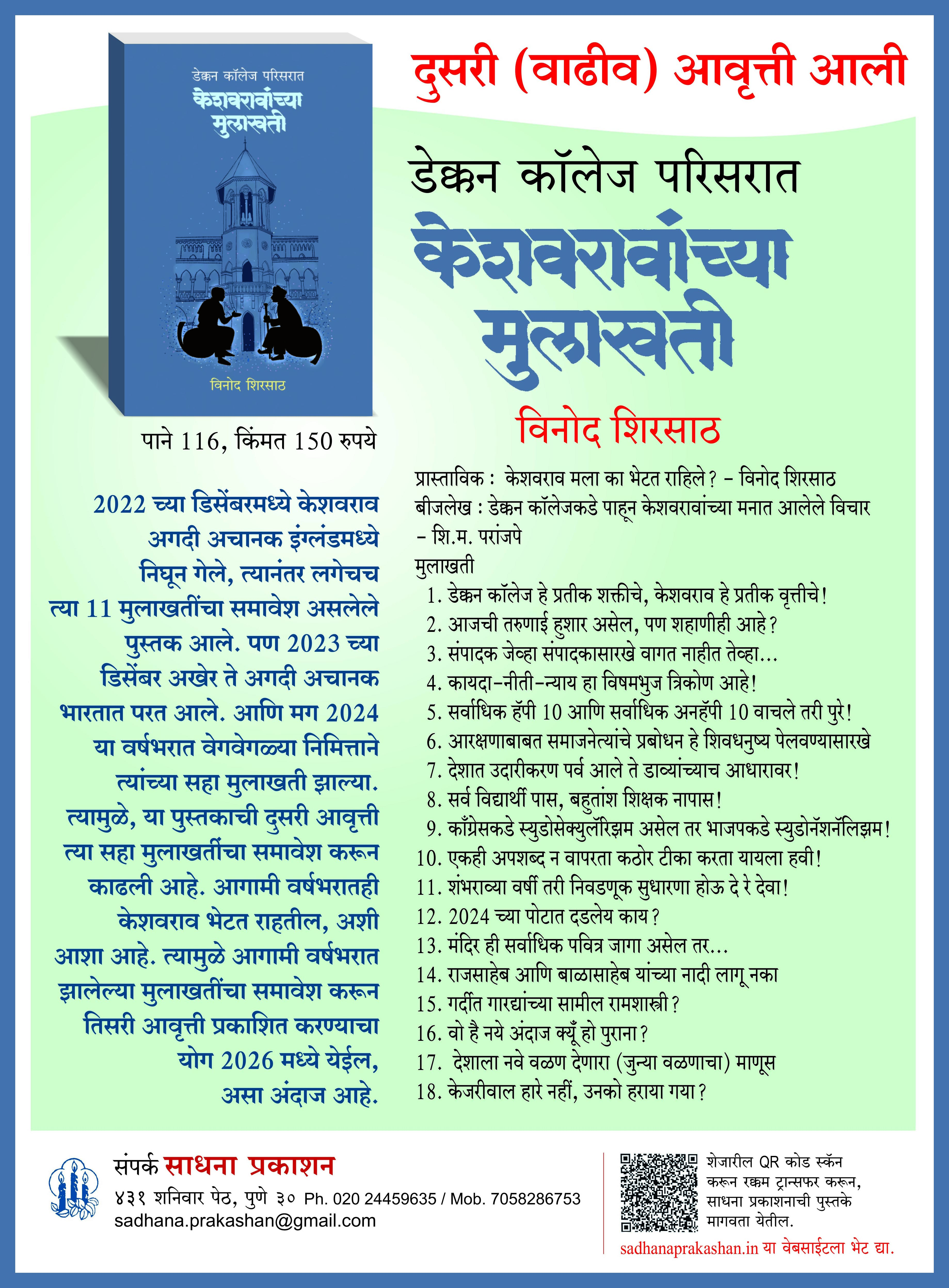
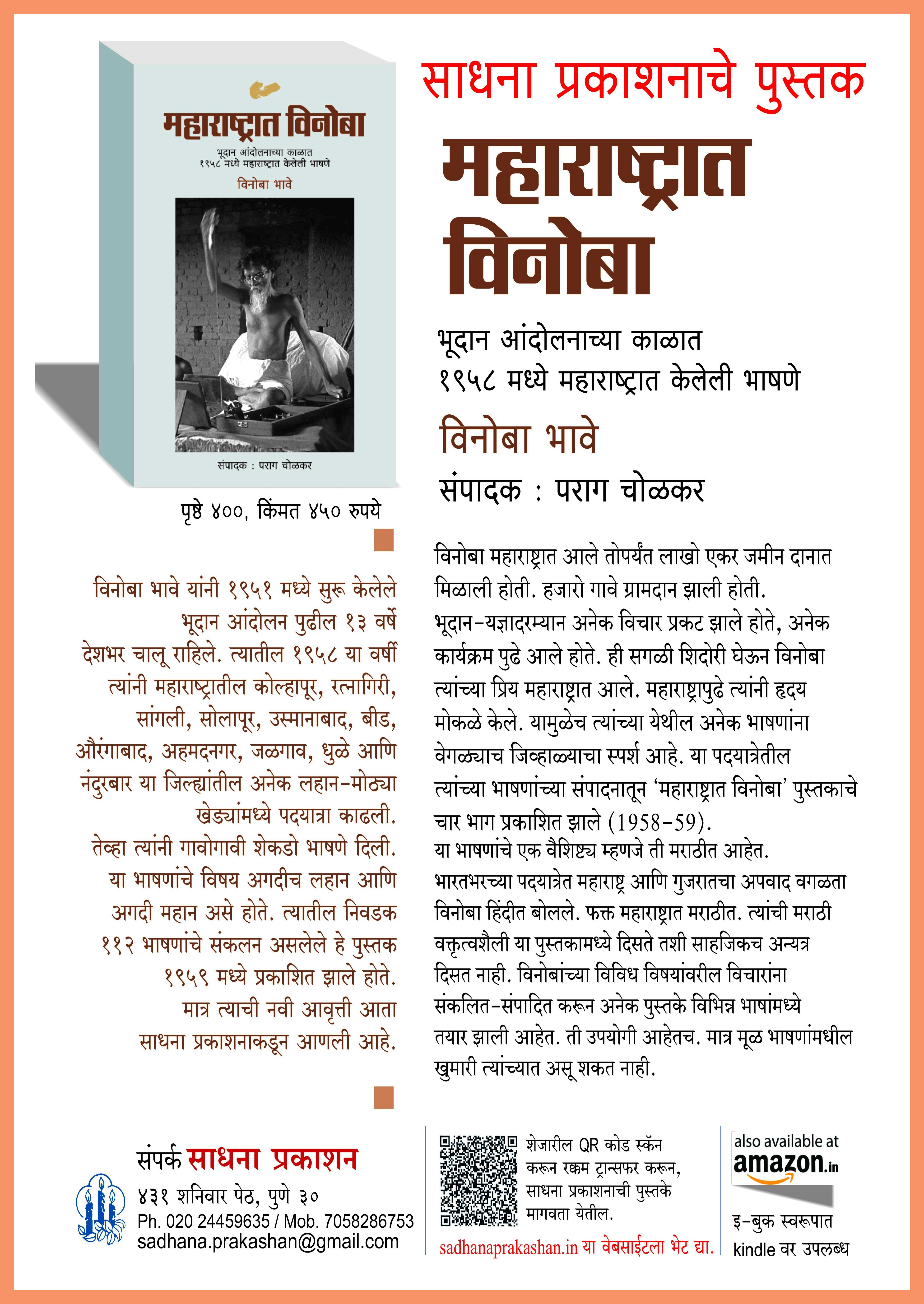

Add Comment